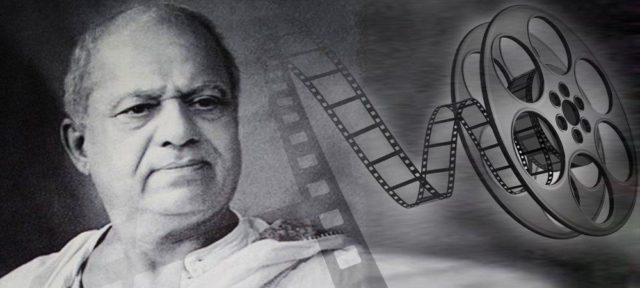दादा साहब फाल्के , जन्म: 30 अप्रैल, 1870, प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता-निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे जो भारतीय सिनेमा के पितामह की तरह माने जाते हैं। दादा साहब फाल्के की सौंवीं जयंती के अवसर पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो आजीवन योगदान के लिए भारत की केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है।
जीवन परिचय
भारतीय फ़िल्म उद्योग के पितामह दादा साहब फाल्के का पूरा नाम ‘धुन्दीराज गोविंद फाल्के’ था किंतु वह दादा साहब फाल्के के नाम से प्रसिद्ध हैं। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल, 1870 को नासिक के निकट ‘त्र्यंबकेश्वर’ में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित और मुम्बई के ‘एलफिंस्टन कॉलेज’ के अध्यापक थे। अत: इनकी शिक्षा मुम्बई में ही हुई। वहाँ उन्होंने ‘हाई स्कूल’ के बाद ‘जे.जे. स्कूल ऑफ़ आर्ट’ में कला की शिक्षा ग्रहण की। फिर बड़ौदा के कलाभवन में रहकर अपनी कला का ज्ञान बढ़ाया।
कार्यक्षेत्र
कुछ समय तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में काम करने के बाद उन्होंने अपना प्रिटिंग प्रेस खोला। प्रेस के लिए नई मशीनें ख़रीदने के लिए वे जर्मनी भी गए। उन्होंने एक ‘मासिक पत्रिका’ का भी प्रकाशन किया। परन्तु इस सबसे दादा साहब फाल्के को सन्तोष नहीं हुआ। सन् 1911 की बात है। दादा साहब को मुम्बई में ईसा मसीह के जीवन पर बनी एक फ़िल्म देखने का मौक़ा मिला। वह मूक फ़िल्मों का ज़माना था। दादा साहब ने फ़िल्म को देखकर सोचा कि ऐसी फ़िल्में हमें अपने देश के महापुरुषों के जीवन पर भी बनानी चाहिए। यहीं से उनके जीवन की धारा बदल गई। आरम्भिक प्रयोग करने के बाद वे लंदन गए और वहाँ पर दो महीने रहकर सिनेमा की तकनीक समझी और फ़िल्म निर्माण का सामान लेकर भारत लौटे। तत्पश्चात् 1912 में ‘दादर’ (मुम्बई) में ‘फाल्के फ़िल्म’ नाम से अपनी फ़िल्म कम्पनी आरम्भ की।
फ़िल्म निर्माण
फाल्के के जीवन में फ़िल्म निर्माण से जुड़ा रचनात्मक मोड़ सन 1910 ‘लाईफ़ आफ़ क्राईस्ट’ फ़िल्म को देखने के बाद आया, उन्होंने यह फ़िल्म दिसंबर के आस-पास ‘वाटसन’ होटल में देखी। वह फ़िल्म अनुभव से बहुत आंदोलित हुए और इसके बाद उस समय की और भी फ़िल्मों को देखा। सिनेमा के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए अत्यधिक शोध करने लगे। इस क्रम में उन्हें आराम का कम समय मिला, निरंतर फ़िल्म देखने, अध्ययन और खोज से फाल्के बीमार पड गए। कहा जाता है कि बीमारी के दौरान भी उन्होंने अपने प्रयोग जारी रखते हुए ‘मटर के पौधे’ के विकास कालक्रम का छायांकन कर फ़िल्म बना दी। कालांतर में इन अनुभवों को फ़िल्म निर्माण में लगाया। फ़िल्म बनाने की मूल प्रेरणा फाल्के को ‘क्राईस्ट का जीवन’ देखने मिली, फ़िल्म को देखकर उनके मन में विचार आया कि क्या भारत में भी इस तर्ज़ पर फ़िल्म बनाई जा सकती हैं? फ़िल्म कला को अपना कर उन्होंने प्रश्न का ठोस उत्तर दिया। फ़िल्म उस समय मूलत: विदेशी उपक्रम था और फ़िल्म बनाने के अनिवार्य तकनीक उस समय भारत में उपलब्ध नहीं थी, फाल्के सिनेमा के ज़रूरी उपकरण लाने के लिए लंदन गए। लंदन में उनकी मुलाकात जाने-माने निर्माता और ‘बाईस्कोप’ पत्रिका के सम्पादक सेसिल हेपवोर्थ से हुई, कहा जाता है कि फाल्के को फ़िल्म सामग्री ख़रीदने में इसी ने मार्गदर्शन किया।[1]
भारतीय सिनेमा के पितामह
धुन्दीराज गोविंद फाल्के (दादा साहब फाल्के) ने फ़िल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखन आदि विविध क्षेत्रों में भारतीय सिनेमा को अपना योगदान दिया था। उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 को बंबई के ‘कोरोनेशन थिएटर’ में ‘राजा हरिश्चंद्र’ नामक अपनी पहली मूक फ़िल्म दर्शकों को दिखाई थी। दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली मूक फ़िल्म बनाई थी। 20 वर्षों में उन्होंने कुल 95 फ़िल्में और 26 लघु फ़िल्में बनाई। दादा साहब फाल्के के फ़िल्म निर्माण की ख़ास बात यह है कि उन्होंने अपनी फ़िल्में बंबई के बजाय नासिक में बनाई। वर्ष 1913 में उनकी फ़िल्म ‘भस्मासुर मोहिनी’ में पहली बार महिलाओं, दुर्गा गोखले और कमला गोखले, ने महिला किरदार निभाया। इससे पहले पुरुष ही महिला किरदार निभाते थे। 1917 तक वे 23 फ़िल्में बना चुके थे। उनकी इस सफलता से कुछ व्यवसायी इस उद्योग की ओर आकृष्ट हुए और दादा साहब की साझेदारी में ‘हिन्दुस्तान सिनेमा कम्पनी’ की स्थापना हुई। दादा साहब ने कुल 125 फ़िल्मों का निर्माण किया। जिसमें से तीन-चौथाई उन्हीं की लिखी और निर्देशित थीं। दादा साहब की अंतिम मूक फ़िल्म ‘सेतुबंधन’ 1932 थी, जिसे बाद में डब करके आवाज़ दी गई। उस समय डब करना भी एक शुरुआती प्रयोग था। दादा साहब ने जो एकमात्र बोलती फ़िल्म बनाई उसका नाम ‘गंगावतरण’ है।
‘हिन्दुस्तान फ़िल्म कंपनी’ की स्थापना
राजा हरिश्चंद्र की कामयाबी के बाद फाल्के ने नासिक जाने का निर्णय लिया। नासिक में आकर फ़ाल्के ने अगली फ़िल्म ‘मोहनी भस्मासुर’ और ‘सावित्री-सत्यवान’ का निर्माण किया। ‘मोहनी भस्मासुर’ में पहली महिला कलाकार दुर्गा खोटे और कमला गोखले ने काम किया। इन फ़िल्मों के हिट होने से फाल्के लोकप्रिय हुए और अब से हरेक फ़िल्म के 20 प्रिन्ट ज़ारी होने लगे, उस समय की परिस्थितियों में यह एक महान् उपलब्धि थी। इन फ़िल्मों में कुशल तकनीक के रुप में ‘स्पेशल इफ़ेक्ट’ अर्थात् विशेष प्रभाव का रचनात्मक प्रयोग हुआ। ‘विशेष प्रभाव’ और ‘ट्रीक फ़ोटोग्राफ़ी’ का प्रयोग दर्शकों के आकर्षण का कारण बना, यह क्रांतिकारी पहल थी। फ़ाल्के तत्कालीन फ़िल्म उपकरणों को लेकर बेहद सजग रहे और सन 1914 में फिर से लंदन गए। लंदन से लौटकर फ़ाल्के ने सन 1917 में नासिक में ‘हिन्दुस्तान फ़िल्म कंपनी’ स्थापित करते हुए अनेक फ़िल्में बनाई। अपने यादगार सफ़र के 25 वर्षों में दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र (1913), सत्यवान सावित्री (1914), लंका दहन (1917), श्री कृष्ण जन्म (1918), कालिया मर्दन (1919), कंस वध (1920), शकुंतला (1920), संत तुकाराम (1921) और भक्त गोरा (1923) समेत 100 से ज्यादा फ़िल्में बनाई। फ़ाल्के पर जार्ज मेलिस का स्पष्ट प्रभाव देखा गया, उनमें दृश्य निर्माण की सुलझी हुई संवेदना के साथ प्रशंसनीय तकनीकी ज्ञान भी था।[1]
प्रमुख फ़िल्में
राजा हरिश्चंद्र (1913)
मोहिनी भस्मासुर (1913)
सावित्री सत्यवान (1914)
लंका दहन (1917)
श्री कृष्ण जन्म (1918)
कालिया मर्दन (1919)
कंस वध (1920)
शकुंतला (1920)
संत तुकाराम (1921)
भक्त गोरा (1923)
सेतु बंधन (1932)
गंगावतरण (1937)
फ़िल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’
मुख्य लेख : राजा हरिश्चंद्र
भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के ने जब भारत की पहली फीचर फ़िल्म बनाने के लिए तैयारी की, तो फ़िल्म की नायिका उनके लिए गंभीर समस्या बन गई। सन् 1913 में बनी फ़िल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ में ‘तारामती’ की विशेष भूमिका थी। फाल्के की इच्छा थी कि नायिका की भूमिका कोई युवती ही करे। इसके लिए पहले उन्होंने नाटक मंडली से जुड़ी अभिनेत्रियों से बात की, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुई। यहां तक कि दादा साहब ने हिरोइन की खोज के लिए इश्तहार भी बंटवाए, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। जब तारामती की भूमिका के लिए अंतत: कोई कलाकार नहीं मिला, तो विवश हो फाल्के कोठे वालियों के पास पहुंचे। उनसे हिरोइन बनने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने भी टका-सा जवाब दे दिया। हारकर दादा साहब ने फैसला किया कि किसी पुरुष से ही तारामती की भूमिका कराई जाए और उसी पल से कलाकार की तलाश शुरू हो गई। तभी एक दिन उन्हें एक ईरानी के रेस्तरां में एक रसोइया नजर आया। दादा ने रसोइया से बात की। कहने-सुनने के बाद वह काम करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन दादा फाल्के की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। दरअसल, रिहर्सल के बाद जब शूटिंग का समय आया, तो निर्माता निर्देशक फाल्के ने रसोइये से कहा – ‘कल से शूटिंग करेंगे, तुम अपनी मूंछें साफ़ कराके आना।’ दादा की यह बात सुनकर रसोइया, जो हिरोइन का रोल करने वाला था, चौंक गया। उन्होंने जवाब दिया- ‘मैं मूंछें कैसे साफ़ करा सकता हूं! मूंछें तो मर्द-मराठा की शान हैं!’ रसोइये की बातें सुनकर दादा फाल्के ने समझाया, भला मूंछ वाली तारामती कैसे हो सकती है? वह तो नारी है और नारी की कोई मूंछ नहीं होती। फिर मूंछ का क्या है, शूटिंग पूरी होते ही रख लेना! काफ़ी समझाने के बाद रसोइया मूंछ साफ़ कराने के लिए तैयार हुआ। वह रसोइया, जो भारत की पहली ‘फीचर फ़िल्म’ की पहली हिरोइन बन रहा था, उसका नाम ‘सालुंके’ था।[2]
सम्मान और पुरस्कार
फाल्के शताब्दी वर्ष 1969 में भारतीय सिनेमा की ओर फाल्के के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में ‘दादा साहब फाल्के सम्मान’ शुरु हुआ। राष्ट्रीय स्तर का यह सर्वोच्च सिने पुरस्कार सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। उनकी स्मृति में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है।
अन्तिम समय
सन 1938 में भारतीय सिनेमा ने रजत जयंती पूरी की। इस अवसर पर चंदुलाल शाह और सत्यमूर्ति की अध्यक्षता में सामारोह आयोजित हुआ, दादा साहब फाल्के को बुलाया तो अवश्य गया किन्तु उन्हें कुछ विशेष नहीं मिला। समारोह में उपस्थित ‘प्रभात फ़िल्मस’ के शांताराम ने फाल्के की आर्थिक सहायता की पहल की पहल करते हुए वहां आए निर्माताओं, निर्देशक, वितरकों से धनराशि जमाकर फाल्के को भेज दिया। इस राशि से नासिक में फाल्के के लिए घर बना। उनके जीवन के अंतिम दिन यहीं बीते।[1] 16 फ़रवरी, 1944 को नासिक में ‘दादा साहब फाल्के’ का निधन हुआ।